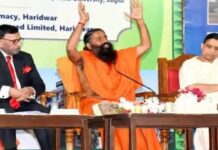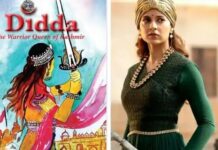इस दिन विशेष कृपा करते हैं सूर्य
लक्ष्मी कान्त द्विवेदी
समाचार सम्पादक
सनातन धर्म में वर्णित तैंतीस कोटि देवी-देवताओं में केवल पांच-विष्णु, शिव, पार्वती, गणेश और सूर्य को मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इनमें भी एकमात्र सूर्य ही ऐसे देवता हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। ‘
‘सूर्योपनिषद’ में कहा गया है, ‘सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’। अर्थात सूर्य इस सम्पूर्ण जगत की आत्मा हैं। इसी में आगे कहा गया है, ‘आदित्याद्वायुर्जायते’, ‘आदित्याद्भूमिर्जायते’, आदित्यादापो जायन्ते’, ‘आदित्याज्ज्योतिर्जायते’, ‘आदित्याद्व्योम दिशो जायन्ते’। अर्थात पंच तत्वों-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। इनमें से कुछ की पुष्टि तो आधुनिक विज्ञान भी करता है। प्रकृति का स्वामी होने के नाते सूर्य को ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप माना गया है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 23 अंश पर झुकी पृथ्वी जब एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो हमें उनके दर्शन आकाश के बारह भागों में होते हैं, जिन्हें बारह राशियां कहा गया है। जब सूर्य किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रान्ति कहा जाता है। वैसे तो सभी संक्रान्तियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें भी चार-मेष, कर्क, तुला और मकर का विशेष महत्व है। इन चारों संक्रान्तियों में भी मकर संक्रान्ति सबसे महत्वपूर्ण मानी गयी है, क्योंकि इस दिन सूर्य सबसे सौम्य रूप में होते हैं और उन पर भी कृपा करते हैं, जिन्हें वह सामान्य तौर पर पसंद नहीं करते।

सूर्यपुराण में कहा गया हैै कि, सूर्य की पत्नी संज्ञा प्रारम्भ में अपने पति का तेज सहन नहीं कर पाती थीं, इसलिए गुप्त रूप से अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गयीं। किन्तु पति को पता न चले, इसलिए अपने स्थान पर अपनी छाया को, जो बोल-चाल, शक्ल-सूरत में हू-ब-हू उन्हीं के जैसी थी, उनके पास छोड़ दिया। सूर्यदेव इस बात से अनजान थे और छाया से उन्हें एक पुत्र शनि हुए। शनि का वर्ण काला होने के कारण सूर्यदेव बचपन से ही उन्हें नापसंद करते थे और उन्होंने उन्हें त्याग दिया था। बाद में भेद खुलने पर उन्होंने छाया को भी त्याग दिया, जिससे शनिदेव और उनके बीच विद्वेष और बढ़ गया। लेकिन मकर संक्रान्ति के दिन सूर्य इतने सौम्य और कृपालु हो गये थे कि, शनिदेव से मिलने उनके घर चले गये। इसी दिन से सूर्य दक्षिणी गोलार्द्ध से उत्तरी गोलार्द्ध की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के करीब आने लगते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि, इसके बाद दिन लम्बे और रात छोटी होने लगेगी। अंधकार के पल घटने और प्रकाश के बढ़ने लगेंगे। भगवान श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि, जो लोग सूर्य के उत्तरायण रहते समय देहत्याग करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसी वजह से भीष्म पितामह ने इसी दिन शरीर छोड़ा था। गंगा भी इसी दिन समुद्र में मिली थीं। पौराणिक आख्यानों के अनुसार, इस दिन स्नान, घ्यान, जप, तप, दान, पुण्य करने से सौ गुने फल की प्राप्ति होती है।
सांसारिक दृष्टि से यह वह समय होता है, जब खरीफ की फसल कट चुकी होती है और रबी की फसल खेतों में लहलहा रही होती है। ऐसे समय में किसान अपने उत्पाद के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करने के साथ-साथ उनसे अगली फसल और अच्छी होने की प्रार्थना करते हैं। यही वजह है कि, यह पर्व केवल भारत ही नहीं, नेपाल आदि अनेक देशों में अपनी भाषा और जलवायु के हिसाब से अलग-अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है। भारत में इसे पंजाब में लोहड़ी, दक्षिण में पोंगल, उत्तर में खिचड़ी तो पूर्वोत्तर में बीहू के नाम से मनाया जाता है। हमारे समझदार पूर्वज रीति-रिवाज तय करते समय हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते थे। वे जाड़े की ठिठुरन से हड्डियों और मटर, गोभी, बैंगन आदि पदार्थों से बनने वाले स्वादिष्ट किन्तु गरिष्ठ व्यंजनों से आंतों पर पड़ने वाले प्रभाव से भलीभांति अवगत थे।
उल्लेखनीय है कि, शरीर में विटामिन डी के भंडारण की क्षमता होती है और यदि इस समय तीन दिनों तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक धूप में रहा जाए, तो शरीर में इतनी मात्रा में विटामिन डी का भंडारण हो जाएगा, जो पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त होगा। इसीलिए इस दिन पतंग उड़ाने की प्रथा शुरू की गयी, ताकि उसी बहाने लोग दिन भर धूप में रहें और उनके शरीर को प्रर्याप्त मात्रा में गर्मी और विटामिन डी मिल सके। यही नहीं कैल्शियम से भरपूर तिल एवं गुड़ से बने लड्डू व गजक, खिचड़ी, दही-चूड़ा, तहरी, मक्के की रोटी-सरसों का साग जैसे सुपाच्य एवं पौष्टिक व्यंजनों का सेवन करने की परम्परा के पीछे भी यही वजह है। इस प्रकार मकर संक्रान्ति भारतीय वांग्मय का पर्व ही नहीं, एक सामाजिक उत्सव भी है।